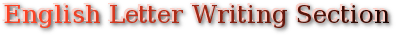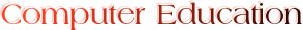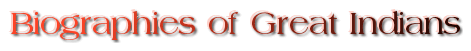Hindi Essay on “Sahitya mein Prakriti Chitran” , ” साहित्य में प्रकृति-चित्रण ” Complete Hindi Essay for Class 10, Class 12 and Graduation and other classes.
साहित्य में प्रकृति-चित्रण
प्रकृति अपने-आप में सुंदर है और मानव-स्वभाव से ही सौंदर्य-प्रेमी माना गया है। इसी कारण प्रकृति और मानव का संबंध उतना ही पुराना है, जितना कि इस सृष्टि के आरंभ का इतिहास। सांख्यदर्शन तो मानव-सृष्टि की उत्पति ही प्रकृति से मानता है। आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत भी इसी मान्यता को बल देता है। अन्य दर्शन पृथ्वी, जल, वायु, अग्रि, और आकाश नामक जिन पांच तत्वों से सृष्टि की उत्पति और विकास मानते हैं, वे भी तो अपने मूल स्वरूप में वस्तुत: प्रकृति के ही अंग है। फिर यह मान्यता भी प्रचलित और प्रसिद्ध है कि साहित्य-सर्जन की प्रेरणा व्यक्ति को प्रकृति के रहस्यमय कार्यों एंव गतिविधियों को देखकर ही प्राप्त हो सकी थी। इस तथ्य में तो तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आरंभ काल में मानव की सहचरी और आश्रय-दात्री सभी कुछ एकमात्र प्रकृति ही थी। उसी की गोद में पल-पुसकर मानव जाति ने जीना एंव प्रगति-विकासकी राह पर चलना सीखा। फलत: वैदिक काल के मानव ने चांद, सूर्य, उषा, संध्या, नदी, वृक्ष, पर्वत आदि प्रकृति के विविध अंग-रूपों को देवत्व तक प्रदान कर दिया था। अनेक पशुओं तथा सांप जैसे जीव में भी देवत्व के दर्शन किए। प्रकृति के प्रति देवत्व का यह भाव आज भी किसी-न-किसी रूप में हमारी अंतश्चेतना ममें अक्षुण बना हुआ है। आज भी हम उसके कईं रूपों की पूजा-अर्चना करते हैं। यह सब कहने का अभिप्राय केवल यह दर्शाना है कि मानव और प्रकृति का संबंध अनादि और चिरंतन है। इसी कारण मानव-जीवन की महानतम उपलब्धि साहित्य और प्रकृति का संबंध भी उतना ही अनादि, चिरंतन और शाश्वत है जितना कि मानव और प्रकृति का।
सभी जानते हैं कि प्रकृति के कोमल-कांत और भयानक मुख्यत: दो ही स्वरूप हैं। ये दोनों स्वरूप प्रत्येक मानव और विशेषकर कवि और साहित्यकार कोटि के मानव को आरंभ से ही भावना का सबल प्रदान करते आ रहे हैं। तभी ताक कवि ने वैदिक साहित्य में यदि प्रकृति को दैवी स्वरूपों में देखा और प्रतिष्ठित किया है, तो परवर्ती कवियों ने उसे उपदेशिका, पथप्रदर्शिका, प्रेमिका, मां, सुंदरी-अप्सरा आदि जाने कितने-कितने रूपों में देखा और चितारा है। आधुनिक काल में आकम सुमित्रानंदन पंत जैसे कवियों ने तो प्रकृति को ही सर्वस्व मानते हुए यहां तक कह दिया है कि-
‘छोड़ दु्रमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया
बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन।’
कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति अपनी सगुण-साकार स्वरूपवता एंव चेतना में आरंभ से ही साहित्यकार के मन-मस्तिष्क पर प्रभावी रही है। उसे सहज सुंदर और शाश्वत की उपासना की प्रेरणा देती आ रही है। हर युग के कवि और साहित्कार ने किसी-न-किसी रूप में प्रकृति का दाम अवश्य ही थामा है। वैदिक साहित्य प्रकृति-चित्रण संबंधी ऋचाओं और सूक्तों से भरा पड़ा है। परवर्ती लौकिक संस्कृत काल का साहित्य भी इसका अपवाद नहीं। कालिदास का ‘मेघदूत’ प्रकति-चित्रण से संबंधित एक अजोड़ काव्य कहा जा सकता है। बाणभट्ट की ‘कादंबरी’ से विशाल, विराट और उदात्त प्रकृति-चित्रण को भला कौन भुला सकता है? संस्कृत में ऐसा एक भी कवि एंव साहित्यकार नहीं हुआ, जिसका मन-मस्तिष्क प्रकृति के रूपचित्रों के चित्रण में न रमा हो। पालि और प्राकृतों के काल में भी मुक्त रूप से प्रकृति-चित्रण साहित्य का अंगभूत रहा। हां, जब हम हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग आदिकाल में आते हैं, तब प्रकृति के उन्मुक्त चित्रण कुछ विलुत्प से होते हुए दिखाई देने लगते हैं। हम पाते हैं कि कविगण मात्र आलंबन या उद्दीपन के रूप मे ंही प्रकृति का आश्रय लेते हैं, मुक्त चित्रण में उनकी रुचि बहुत कम दिख पड़ती है। स्पात तब के कवियों के लिए प्रकृति के मुक्त निरीक्षण-वर्णन के लिए उपयुक्त अवसर ही नहीं रह गया था। यही बात भक्ति और रीतिकाल के बारे में भी एक सीमा तक सत्य कही जा सकती है। फिर भी प्रकृति ने मानव और साहित्य का साथ कभी छोड़ा नहीं, यह निभ्र्रान्त सत्य है। षड्ऋतु-वर्णन, बारहमासा आदि के रूप में इन कालों में, विशेषत: महाकाव्यों आदि में प्रकृति-चित्रण होता ही रहा है। आदिकाल में रचे गए ‘पृथ्वीराज रासो’ में प्रकृति चित्रण का एक उदाहरण देखें:
‘मानहुं कला ससिभान कला सोलह सों बन्निय।
बाल बैस ससि ता समीप अभ्रित रस पिन्निय।।’
इस काल में रची गई विद्यापति तथा अन्य कवियों की कविता में भी आलंबन-उद्दीपन रूप में यत्किचित प्रकृति चित्रण मिल जाता है। परवर्ती भक्तिकाल के साहित्य में जायसी और तुलसीदास के काव्यों में प्रकृति के प्राय: सभी रूपों के उन्मुक्त दर्शन होने लगते हैं। वहां प्रकृति मानव के सुख-दुख की सहभागिनी भी बनती हुई दिखाई देती है। तभी तो जायसी की रानी नागमती की विरह-दशा सी पीडि़त होकर- ‘आधी रात पपीहा बोला’ और सीता-हरण के बाद श्रीराम के मुख से इस प्रकार के उक्तियां सुनने को मिलती हैं :
‘हे खग-मृग है मधुकर स्नेनी। तुम देखी सीता मृगनैनी।’
इतना ही नहीं, उमड़ घुमडक़र आते बादलों को देख श्रीराम लक्ष्मण से कह उठते हैं:
‘घन घमंड गरजत नभ घोरा। प्रियाहीन मन डरपत मोरा।’
इस प्रकार भक्तिकाल के साहित्य में प्रकृति के सघन और मानव-संबंद्ध अनेक रूप देखे जा सकते हैं। रीतकाल में भी प्रकृति-चित्रण मुख्यत: आलंबन रूप में ही हुआ है, पर बिहारी आदि की कविता में उसका उन्मुक्त सरस चित्रण भी देखा जा सकता है। राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करता है। इसी प्रकार जब कोई वैदिककालीन कवि यह कल्पना करता है कि:
‘संगच्छध्वं संवद्ध्वं, संवो मनांसि जानताम’
अर्थात संपूर्ण राष्ट्र जन एक साथ मिलकर चलें, अपनी बाणी से एक ही तत्व की बात कहें और सबके समान शिव की बात सोंचेंगे, तो निश्चय ही वह राष्ट्रीयता की व्यापक भावना काा ही प्रतिपादन कर रहे होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य में आरंभसे ही राष्ट्रीयता का महत्व, उसकी स्वतंत्र आवश्यकता आदि के महत्व का प्रतिपादन होता आ रहा है। निश्चय ही वह कवि महान राष्ट्रीय भावना से ही परिचालित था, जिसने कहा :
‘जननी जनै तो भक्त जन, या दाता या शूर।
अखै तौ जननी बांझ रहि, काहे गंवावै नूर।’
इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना ही किसी एक भू-भाग के निवासियों को परस्पर संबद्ध रखा करती है, यह बात स्पष्ट है। मातृभूमि पर मिटने की प्रेरणा दिया करती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि इस बात को भली प्रकार समझते थे, इसी कारण संकुचित स्तर पर ही सही, वे लोग अपने आश्रयदाताओं की राष्ट्रीय भावनाओं की हमेशा उद्दीप्त रखते रहे। उसी युग के आल्हाकार ने ही तो राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से अनुप्राणित हो यह कहा था :
‘बारह बरसि लै कूकर जीयें, और तेरह लै जियें सियार।
बरसि अठारह छत्री जीयें, आगे जीवन को धिक्कार।’
कवि के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आदिकालीन साहित्य-सृजन का मूल प्रेरणा-स्त्रोत राष्ट्रीयता का जागरुक उदात्त भाव ही था। आगे चलकर भक्तिकालीन साहित्य में राष्ट्रीयता का भाव सूक्ष्म एंव तरलायित होकर अन्य प्रकार से अभिव्यक्त होने लगा। कबीर, तुलसी, जायसी आदि सभी कवियों की वाणी से जिस भावनात्मक एंव भक्ति-क्षेत्र में समानता-समन्वय का संदेश मिलता है। निश्चय ही वह राष्ट्रीय एकता को अक्षुण रखने का प्रयत्व है। तदनंतर रीतिकाल के श्रंगार-दूषित वातावरण में भी महाकवि भूषण, गोरेलाल, सूदन और गुरु गोविंद सिंह जी की कविता का एक उदाहरण देखें कि जिसमें राष्ट्र के लिए मर मिटने की अदम्य लालसा प्रकट की गई है :
‘देहु शिवा? वह मोहि इहै शुभ कर्मन तैं कबहूं न टरौं।
न डरौ अरि सों अब जाइ लरौं निशचै करि आपुनि जीत करौं।।
अरु सिक्ख हौं आपने ही मन को इह लालच हौं गुन तौं उचरौं।
जब आव की औध निदान बनै अति ही रण में तब जूझि मरौं।’
राष्ट्रीयता एक पवित्र परंपरा है और उसके गुणगान की परंपरा भी युग-स्थितियों के अनुकूल अनवरत वृद्धि पाती जाती है। कवि और साहित्यकार शाश्वत सत्यों के गायक एंव रक्षक होते हुए भी अपने युग का प्रतिनिधित्व अपनी रचनाओं में अवश्य किया करते हैं। तभी तो मध्य काल के बाद परतंत्रता के परिवेश में जब आधुनिक काल का आरंभ हुआ तो आधुनिक काल के प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्वर चिंतित हो उठा :
‘अंगरेज राज सुख-साज सजे सबै भारी
पै धन बिदेश चलि जात, यहै अति ख्वारी।’
इस ख्वारी से आहत होकर वे भारतवासियों का आहवान कर कह उठे :
‘आवहुं सब मिलि रोवहुं भारत भाई,
हा-हा भारत दुर्दशा न देखि जाई।’
और राष्ट्रोद्धार के लिए वे जनता के साथ-साथ भगवान को भी सोते से जगाने लगे। अन्य युगीन कवि भी राष्ट्र-भावना से विमुख न रहकर इसके जागरण एंव उत्थान के लिए अपनी भावनाओं की वाणी देते रहे। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का समूचा काव्य राष्ट्रीयता का उदगान है। सत्यानायण कविरत्न, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां किस राष्ट्र पे्रमी के मन-मस्ष्कि को झनझना नहीं देती :
‘मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक।’
यहां तक कि छायावादी कवि भी अपने-आपको राष्ट्रीयता की भावना से विलग न रख सके। प्रकृति के माध्यम से भी राष्ट्र-भावना को प्रश्रय देते रहे :
‘अरुण यह मधुमय देश हमारा
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।’
आज भी भारत की सभी भाषाओं, विशेषकर हिंदी भाषा के सजग साहित्यकार युगानुरूप राष्ट्रीयता की पहचान बना रखने की दिशा में अपनी ओजस्वी वाणी निरंतर मुखरित करते रहे और कर भी रहे हैं। दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, वियोगी हरि, श्यामनारायण पांडे आदि ने तो इस भावना कीी अंत-सलिला को प्रवाहमान रखा ही, अन्य अनेक कवि और लेखक भी मुख्यत: राष्ट्रीय भावनाओं को ही अपने साहित्य में सजा-संवारकर प्रगट कर रहे हैं। आने वाली पीढिय़ां भी इस सरिता की धारा को सूखने न देकर सतत प्रवाहित रखेंगी, ऐसी आशा की जा सकती है।
वस्तुत: कोई देश गुलाम हो सकता है, पर मन-भावों के संबंध रखने वाली राष्ट्रीयता की भावना कभी भी न तो गुला हुआ करती है औन न ही कभी मर ही सकती है। प्रत्येक युग के जागरूक साहित्यकारों की वाणी उसमें नव-रक्त का संचार कर उसे जगाए तो रखती ही है, आगे भी बढ़ा दिया करती है। मानव-सृष्टि के आरंभ से ही यह क्रम चलता आ रहा है और अनंतकाल तक चलता रहेगा। भारत आदि कई देशों द्वारा स्वतंत्रता को खोकर देर-सवेर उसे फिर प्राप्त कर लेना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है।