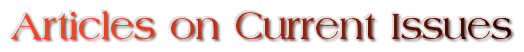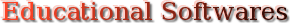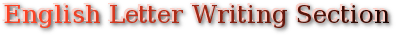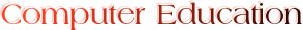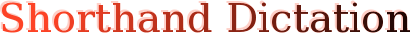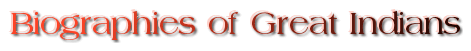Hindi Essay on “Vahi Manushya he ki jo Manushya ke liye Mare”, “वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे” Complete Hindi Nibandh for Class 10, Class 12 and Graduation.
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे
Vahi Manushya he ki jo Manushya ke liye Mare
प्रस्तावना : पारस्परिक सहयोग का मानव-जीवन में विशेष महत्व है। इस सद्भावना के अनेक रूप हमें विश्व में दृष्टिगत होते हैं। कहीं पर यह पारस्परिक सहयोग स्वार्थपरता पर अवलम्बित है, तो कहीं धूर्तता और कूटनीति का चोला पहने हुए है और सहयोग में बदले की भावना भी रहती ही है। यह सद्भावना ही उपकार के नाम से भी अभिहित की जाती है। वास्तव में जो कार्य विशेष परिस्थिति में किए जाते हैं, वे उपकार कहलाते हैं; किन्तु जो बदले की भावना से अलग होकर सिर्फ परहित के लिए किए जाते हैं, वे परोपकार कहलाते हैं। इन कार्यों में स्वार्थ की भावना का सदैव अभाव रहता है। दूसरे की शोचनीय अवस्था करुणा उपजा जाती है, यह सहानुभूति को जन्म देती है और इससे परोपकार की प्रेरणा आ जाती है। आज के युग में मानव का सबसे बड़ा गुण है-परोपकार। इसका शब्दिक अर्थ है दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना । अतः राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने कहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे इस काव्योक्ति में मानवता का लक्ष्य दर्शाया गया है।
काव्योक्ति का तात्पर्य : इस काव्योक्ति का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए तत्पर होता है और उसी के लिए काया धारण रखता है अर्थात् उसी के लिए मरता-जीता है, वही वास्तव में मनुष्य है। यहाँ पर मनुष्य का अर्थ उससे है जो मानवता के वास्तविक गुणों से विभूषित है। सच्चा मनुष्य वही है जो जन-कल्याण के लिए अपने प्राण तक कुर्बान कर सकता है। बहुधा सभी महत्त्वाकांक्षी जन-कल्याण के लिए उद्यत होते हैं; पर इनमें से अधिकांश छोटा-सा कार्य करके बड़ा श्रेय पाना चाहते हैं; पर वास्तविक मनुष्यों का जीना-मरना जनहित के लिए ही होता है।
उदाहरणों द्वारा पुष्टि : परोपकारी मानव में मानवीय गुणों का समावेश हो जाता है। पुरातन युग में शिवि नामक एक बहुत ही परोपकारी राजा हुआ था। उन्हें किसी व्रत का अनुष्ठान प्राप्त था। उनकी गोद में। घायल और डरा हुआ एक कबूतर आकर बैठ गया। महाराज शिवि ने उसे प्यार से अपनी शरण में रख लिया। तत्काल ही एक बाज उसका पीछा करता हुआ वहाँ पर पहुँचा और महाराज शिवि से कबूतर को माँगने लगा। उन्होंने अपने शरणागत कबूतर को देने से मना कर दिया। इस पर बाज ने कहा कि महाराज ! आप धर्मात्मा हैं और यह कबूतर मेरा भोजन है। मैं कई दिवस से भूखा हूँ। अत: यदि आप इसे मुझे नहीं देंगे; तो मैं भूखा रहकर यहीं प्राण त्याग दूंगा। इस पर महाराज शिवि ने उत्तर दिया कि हे बाज ! यह डरा हुआ पक्षी मेरा शरणागत है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
अत: इसे छोड़कर जैसे मी तुम्हारी क्षुधा मिट सके, वह उपाय बताओ। इस पर बाज ने तत्काल ही जवाब दिया कि महाराज ! यदि आप इस कबूतर के बराबर अपनी देह का माँस दें, तो मेरी क्षुधा मिट सकती है। बाज की बात सुनकर महाराज शिवि तत्काल तैयार हो गये और कबूतर को तराजू के पलड़े में रखकर दूसरे पर अपनी देह से काट-काटकर माँस रखने लगे। लगभग सारा माँस काटकर उस पर रख दिया फिर भी वह कबूतर के वजन को पूरा न कर सके। तत्पश्चात् महाराज स्वयं तराजू पर चढ़ गए। तब कहीं कबूतर के भार के बराबर हो सका। यह देख, चन्द्र और अग्नि ने जो कबूतर और बाज के रूप में आ गए थे, महाराज शिवि की सराहना करने लगे और उन्हें वरदान देकर अन्तर्धान हो गए। इस तरह धर्मपरायण नरेश शरणागत पक्षी की रक्षार्थ प्राण न्योछावर भी कर सकते थे। ऐसे लोग देव तुल्य समझे जाते हैं। इस तरह के अनेक उदाहरणों से हमारे ग्रन्थ भरे पड़े हैं।
मनुष्य यदि अपने बन्धु-बांधव की सहायता नहीं कर सकता है। तो उसमें और पशु में अन्तर ही क्या रह गया है। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। मनुष्य वही है जो दूसरों का पेट भरता है, दूसरों के दु:खों का निवारण करता है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो अधिक गिरे हुए हैं। हमारा मनुष्य योनि में आना व्यर्थ है। हम ऐसी स्थिति में पशु से भी आज के युग में राष्ट्रपिता, नेताजी, शांतिदूत जवाहर और जननायक शास्त्री जी आदि अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जनहित के लिए अपनी सुख-सुविधाएँ त्याग दीं। अनेक प्रकार के कष्टों को सहन किया। ऐसे लोग महापुरुष कहलाए। इसी तरह महर्षि दयानन्द और महर्षि श्रद्धानन्द आदि अनेक महात्माओं ने जन-कल्याण के लिए आत्म-बलिदान किया है। ऐसे ही महापुरुषों में वास्तविक मानवता के दर्शन होते हैं।
लाभ और प्रभाव : स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों में और शहीदों में, कौन-सी भावना थी जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। जानते हो, वह थी स्वाभिमान और जन-कल्याण की भावना। इसका उनमें प्रबल प्रभाव था। इस तरह के महान् व्यक्तित्व का आज भी अभाव नहीं है जो मनुष्य के लिए जीते मरते हैं। एक मनुष्य को भी यदि वास्तविक लाभ पहुँचाया जा सका, तो उसी में सफलता है। जो मनुष्य दूसरों के लिए बलि देने को तैयार रहते हैं, उनके लिए भी बलिदान देने वाले मिल जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के कार्यों की एक परम्परा-सी बन जाती है जिससे प्रभावित होते रहते हैं और इस तरह से समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि किसी को भी आपत्काल में निराश्रयता का अनुभव नहीं होता। सभी न्याय की राह पर चलने का प्रयत्न करते हैं। इससे समाज का पूर्णतया विकास हो है। मानवता को परखने की यह वास्तविक कसौटी है।
उपसंहार : मानवी जीवन सार्थकता ही परोपकार में निहित है और मानवीय गुणों का समावेश इसमें रहता है। अत: गुप्त जी की यह काव्योक्ति कि ‘वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।’ नितान्त उचित एवं सत्य है। मनुष्य के लिए दूसरों के हित में मरना-जीना ही सबसे बड़ी मानवता है।