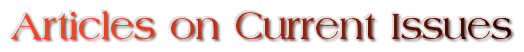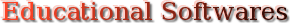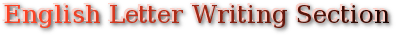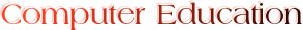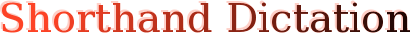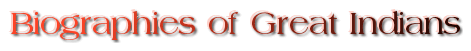Hindi Essay on “Shath Sudhrahi Satsangati Pai”, “शठ सुधरहिं सत्संगति पाई” Complete Hindi Nibandh for Class 10, Class 12 and Graduation and other classes.
शठ सुधरहिं सत्संगति पाई
Shath Sudhrahi Satsangati Pai
प्रस्तावना : यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के अनुसार कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अत: वह अकेले रहना नहीं चाहता है, उसे साथ चाहिए, वह संगति की अपेक्षा करता है। मानव को संगति चयन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बड़ा सोच-विचार कर साथियों का चयन बच्चे को बचपन ही से कराना चाहिए; क्योंकि एक बार जो संस्कार पड़ जाते हैं, वे फिर आसानी से समाप्त नहीं होते हैं। यही कारण है कि संगति के विषय में प्राचीन और अर्वाचीन सभी विचारकों ने बड़ी गम्भीरता के साथ चिन्तन किया तथा संगति की महिमा का वर्णन किया है। कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगति का वर्णन बड़ा विस्तारपूर्वक किया है। एक स्थान पर वह कह उठे-
“तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग।
तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग।।”
कवि की इस युक्ति में वास्तविकता है।
जो स्वर्ग इतना महान् है कि स्वर्ग तथा मोक्ष आदि का सुख भी उसकी समानता नहीं कर सकता, आखिर वह सत्संग है क्या ?
सत्संग का अर्थ : ‘सत्संग’ शब्द सत् + संग से बना है। सत् का अर्थ सज्जन एवं संग का अर्थ है साथ। अतः सज्जन लोगों की संगति सत्संगति या सत्संग कहलाता है। शिष्ट, सहृदय एवं परोपकार आदि से युक्त जो सज्जन होते हैं, उन्हीं का साथ करना चाहिए। विस्तृत अर्थों में केवल साथ रहने मात्र ही का नाम सत्संग नहीं हो सकता। यदि संगति से लाभ नहीं हुआ, तो वह वैसे ही है जैसे चित्र में बने। प्रेम-रहित होने पर लोगों की आकृतियाँ चित्रवत् हैं और उनकी बातें अर्थ रहित हैं। अत: यह सिद्ध हुआ कि संगति के लिए प्रेम का होना परमावश्यक है। यदि मनुष्य सच्चे अर्थ में संगति की कामना करना चाहता है, तो उसे प्रेमभाव को अपनाना होगा।
सज्जनों के सद्गुण : जहाँ दुर्जन अवगुणों की खान एवं नर्क दर्शन कराने वाले होते हैं, वहीं सज्जन सद्गुणों का भण्डार होते हैं तथा वे स्वर्ग के दर्शन इंसी भू पर करते हैं। सज्जन अपने हानि या लाभ की चिन्ता न करके दूसरों का हित साधन करते हैं। सज्जनों का धन व विद्या परोपकारार्थ होती है। ऐसे ही सज्जनों के लिए तुलसी ने कहा-
परहित लागि तजहिं जो देही। सन्तन संत प्रशंसहिं तेही।।”
सज्जन दूसरों को सुखी देखकर मुदित (प्रसन्नता की भावना से युक्त) तथा दूसरों को दु:खी देखकर करुणा से युक्त होते हैं तथा ऐसे सन्त, “पर दु:खे उपकार बहुत जे मन अभिमान न आने रे।” दुष्ट व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है; किन्तु सज्जन अपने मुख पर अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनने के अभ्यस्त नहीं होते हैं तथा मन में। स्वाभिमान होते हुए भी अभिमान नहीं करते तथा सर्वदा दूसरों के सम्मुख अपने छोटा एवं अज्ञानी ही बतलाते हैं।
सत्संगति का महत्त्व : ‘संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति’ के कथनानुसार संगति के प्रभाव से ही दोष व गुण उत्पन्न होते हैं। दुष्टों की संगति करने से दुर्गुण आते हैं और सज्जनों के सम्पर्क से हम महान् बन जाते तथा हमारा महत्व बढ़ जाता है, जैसा कि इन्हीं भावों को इस कथन में व्यक्त किया गया है।
संगति ही गुण ऊपजै, संगति ही गुण जाय।
बाँस फाँस औ भीतरी, एकै भाव निकाय।”
एक छोटा-सा पैरों तले कुचला जाने वाला कीट भी पुष्प की संगति से महान् पुरुषों तथा देवों के सिर पर वास पाता है। काँच का टुकड़ा सोने के आभूषण में मरकत मणि जैसी द्युति को धारण करता है। इसी प्रकार कमल के पत्तों के ऊपर पड़ा जल मोती के समान शोभायमान होता है। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के सम्पर्क से कीचड़ में मिल जाती है। सत्संग से व्यक्ति कुछ का कुछ बन जाता है। इस विषय में किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य नहीं करना चाहिए; क्योंकि सत्संगति का महत्त्व सर्वविदित है जैसा कि महात्मा तुलसीदास ने अपना मत अभिव्यक्त किया है-
“सुनि अचरज करै जनि कोई। सत्संगति महिमा नहिं गाई।।”
सत्संग में रहने से मानव को उसकी हीन वृत्तियाँ नहीं सता पाती। हैं। विश्वविख्यात, साहित्य-सृष्टा व मानवतावादी लेखक टालस्टाय ने एक स्थान पर लिखा है कि जंगली जानवरों का रक्त सदा ही मानव में रहता है। लेखक का कथन सत्य है और इस जंगली रक्त के प्रभाव को बचाना सत्संगति का ही काम है। इस कारण भी सत्संग को बड़ा महत्त्व दिया गया है।
सत्संगति के उदाहरण : सत्संग के प्रभाव से दुष्प्रवृतियों वाले बड़े-बड़े दानव भी देवता बन जाते हैं। कौन नहीं जानता कि कुख्यात व दुर्दान्त डाकू अंगुलिमाल महात्मा बुद्ध की संगति से ही सहृदय तथा महान् मानव बन गया था। वह वंही डाकू था जिसे पकड़ने में सरकार की सम्पूर्ण सेना भी मात खा चुकी थी। महान् आदिकवि वाल्मीकि के नाम से कौन अनभिज्ञ है। यही वाल्मीकि प्रा में कुख्यात तथा दुर्दांत लुटेरे थे। सज्जन मुनियों के उपदेश से उनको वैराग्य हुआ और घर बार छोड़ कर उन्होंने राम के उल्टे नाम ‘मरा- परा’ का जाप किया। जिससे वे कवि के शब्दों में-
“उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना।”
इस पूर्वकाल के अमर वाल्मीकि के अतिरिक्त नारद तथा अगस्त्य जो ने भी अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त के द्वारा सत्संग के महत्व को बतलाया है। जैसा कि सन्त कवि तुलसीदास का रामचरितमानस में संकेत है-
वाल्मीकि नारद घटयोनी। निज तिज मुखन कही निज होनी।।”
निरक्षर कबीरदास सत्संग के प्रभाव ही से न केवल कवि अपितु महान् रहस्यवादी दार्शनिक बन गए और उन्होंने सत्संग का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण कुसंग की बुराई व्यक्त करते हुए किया है-
“नारी की झाँई पड़े अन्धा होत भुजंग।
ते नर कैसे जियें जे नित नारी के संग।।”
सत्संग के प्रभाव से ही अनेक कठोर सम्राट देवतुल्य बन गए। सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता जिन्होंने महाभयानक कलिंग युद्ध किया था जिसमें शोणित के सागर उमड़ पड़े थे। लाशों के ढेर लग गए थे; किन्तु उनकी हिंसा की प्यास बुझ न सकी थी। वे ही उपगुप्त की संगति में आकर महामानव ही नहीं अपितु देवतुल्य बन गये।
कुसंगति का प्रभाव : जिस प्रकार सत्संगति की महिमा अनन्त है, उसी प्रकार कुसंगति का प्रभाव भी कम नहीं है। कुसंगति को सबसे भयानक ज्वर कहा गया है। यह ऐसा ज्वर है जो रोगी को घुन की तरह धीरे-धीरे नष्ट करता है। यह मीठा विष है जिसका परिणाम दारुण यन्त्रणा है। असज्जन बिना प्रयोजन के ही अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों की हानि देखकर जिन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। यह दुष्ट दूसरों के छोटे दोषों को भी देख लेते हैं। और अपने बड़े-बड़े दोषों पर भी दृष्टिपात नहीं करते जैसा कि इस नोति वचन में कहा गया है
“खलः सर्षपमात्राणि परछिद्राणि पश्यन्ति।
आत्मनः विल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यन्ति।।”
दुष्टों की संगति से सज्जन से सज्जन व्यक्ति दूसरों के हित का घातक बन जाता है। दुष्टों का उदय पुच्छल केतु के समान अनिष्टकारी होता है। यह दुष्टजन अपना शरीर त्याग करके भी दूसरों का अहित करने का पाठ पढ़ाते हैं-
पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं।
जिमि हिम उपनकृषी दलि गरहीं।।”
‘गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है’ वाली कहावत के आधार पर दुष्टों के साथ से न केवल हमारे विचार और चरित्र दूषित होते हैं; अपितु कभी-कभी तो बुरा कार्य करते हैं। दुष्ट व्यक्ति और फल हमको भोगना पड़ता है। उदाहरण मौजूद है कि रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण किया; परंतु उसके सामीप्य से समुद्र को बँधना पड़ा।
इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है। कि अनेक युवराज अपने राज्य से हाथ धो बैठे । इसे सब जानते हैं; किन्तु दु:ख का विषय है कि आज भी अनेक युवक-युवतियाँ कुसंगति के शिकार बन जाते हैं। फलत: वे अपने गुरुजनों तथा शुभेच्छुकों का अपमान करते हैं। बुरा कार्य करने को बड़ा समझते हैं और अन्त में उनको करुणापूर्ण दुर्भाग्य का मुख देखना पड़ता है। अतः कुसंगतिसे सर्वदा बचना चाहिए। अपने को चतुर समझकर कुसंगति के पंक मे नहीं धंसना चाहिए, मे नहीं धंसना चाहिए क्योंकि-
“काजल की कोठरी में कैसी ही सयानी जाय।
एक लीक काजर को लागि है, पै लागि है।”
सत्संगति से लाभ : जहाँ दुर्जनों की संगति हमें पाप पंक में डालती है वह सज्जनों की संगति से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सन्तों का समाज संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। जिस प्रकार प्रयाग में स्नान करने से हमारे कालुष्य धुल जाते हैं, उसी प्रकार आत्म संस्कार रूपो तुरन्त फल देने वाला यह सज्जनों का सामीप्य रूपी प्रयाग है जैसा कि मानसकार ने व्यक्त किया है-
“मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीर्थराजू।।”
सत्संगति से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। हमें सर्व प्रकार के सुख भी सत्संगति से ही प्राप्त होते हैं। सन्तोष रूपी धन हम सत्संगति से ही प्राप्त करते हैं। सत्संगति से हमारे अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। सत्संगति हमें बताती है कि प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। अत: हम भली प्रकार नीति की पुस्तकों की संगति से परख लेते हैं कि-
“नारिकेल समाकार दृष्यन्ते भुवि सज्जना।
अन्ये च वदिरिकाकारा वहिरैव मनोहरा।।”
हम सत्संगति से ही सच्चे मित्र की पहचान का ज्ञान प्राप्त करते
“रहिमन सम्पत्ति के सगे बनत बहुत बहु रीति।।
विपति कसौटी जे कसे सोई साँचे मीत।।”
अधिक विस्तार न करके संक्षेप में सत्संगति मनुष्य के लिए आखिर क्या नहीं करती ? सभी वह हमारी बुद्धि की मूर्खता का हरण करती है, सत्य बोलना सिखाती है, चित्त को प्रसन्न रखती है तथा सम्पूर्ण दिशाओं में हमारे यश का विस्तार करती है।
उपसंहार : सज्जन स्वयं कष्ट सहन कर भी दूसरों के दोषों को छिपाते हैं। सज्जन सभी श्रेष्ठ गुणों की खान हैं। इस भौतिकवादी युग में भी विवेकी जन ही ख्याति पाते हैं और ‘बिनु सत्संग विवेक न होई’ यह सत्संगति न केवल विवेक दात्री अपितु आनन्द तथा कल्याण दात्री होने के साथ ही हमको धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष सभी फलों की प्राप्ति का साधन है, जैसा कि सन्त तुलसी का वक्तव्य है-
“सत्संगति मुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला।।”
अत: सत्संग जीवन है कुसंग मृत्यु है। जब निष्प्राण पारसमणि के प्रभाव से बुरे से बुरा लोहा भी अच्छी धातु के रूप में बदल जाता है तो सजीव दुष्ट जन पर सत्संगति का प्रभाव क्यों न पड़े। जहाँ ‘काक होहिं पिक बकउ मराला’ जैसी संत तुलसी के हृदय में आस्था है वहीं सत्संगति के विषय में उनका निश्चयपूर्वक यह कथन बड़ा ही सत्य है।
“सठ सुधरहिं सत्संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई।।”
अत: लौकिक सुख एवं पारलौकिक मोक्ष व शान्ति प्राप्ति के लिए हमें सत्संगति ही करनी चाहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है।