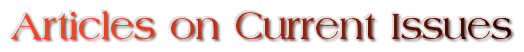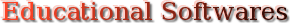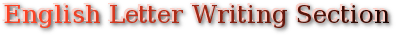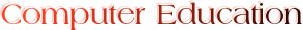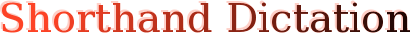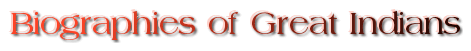Veer Ras Ki Paribhasha, Bhed, Kitne Prakar ke hote hai aur Udahran | वीर रस की परिभाषा, भेद, कितने प्रकार के होते है और उदाहरण
वीर रस की परिभाषा
Veer Ras Ki Paribhsha
परिभाषा – सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तब वीर रस की निष्पत्ति होती है।
शत्रु, अधर्म या दरिद्रता की बढ़त देखकर उसे परास्त करने के निमित्त कठिन से कठिन प्रयास के प्रति उत्पन्न होने वाले उत्साह के भाव को ही वीर रस का सूचक माना जाता है। यह वीरता या उत्साह चार प्रकार का हो सकता है –
(1) युद्धवीर, (2) धर्मवीर, (3) दानवीर, (4) दयावीर
स्थायी भाव – उत्साह, विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए कठिन से कठिन कार्य का उत्साह ।
आलम्बन विषय – शत्रु, अधर्म, दरिद्र तथा दीन व्यक्ति।
आश्रय – वीर व्यक्ति ।
उद्दीपन विभाव – शत्रु की ललकार, मारु बाजे, धार्मिक आख्यान, यश पाने की इच्छा, दीन व्यक्ति की दीनता।
अनुभाव – बाहु संचालन, अपने बल का वर्णन, धर्म-रक्षा का प्रयास, दान देना, मधुर शब्द कहना, उदारता दिखलाना, धैर्य बँधाना, आश्वासन देना आदि।
संचारी भाव – हर्ष, उत्सुकता, धैर्य, वितर्क आदि ।
(1) युद्धवीर के उदाहरण –
हे सारथे! हैं द्रोण क्या, देवेन्द्र भी आकर अड़े।
है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े।
मैं सत्य कहता हूँ सखे! सुकुमार मत जानो मुझे,
यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। (जयद्रथ वध)
यहाँ स्थायी भाव – उत्साह, आश्रय – अभिमन्यु, विषय – द्रोणाचार्य, अनुभाव – अभिमन्यु की दर्पोक्तियाँ, उद्दीपन – चक्रव्यूह की रचना, संचारी भाव = व्यग्रता, आवेग ।
सौमित्र को घननाद का रव अल्प भी न सहा गया गया।
निज शत्रु को देखे बिना उनसे न तनिक रहा गया।
रघुवीर के आदेश से, युद्धार्थ वे सजने लगे,
रणवाद्य भी निर्घोष करके, धूम से बजने लगे।
यहाँ स्थायीभाव उत्साह, आश्रय = लक्ष्मण, विषय = मेघनाथ (शत्रु), अनुभाव – शस्त्र धारण करना, युद्ध के लिये सजना, उद्दीपन मेघनाथ की गर्जन, रणवाद्य, संचारी भाव = व्यग्रता, आवेग ।
अन्य उदाहरण हैं-
आज सिंधु ने विष उगला है,
लहरों का यौवन मचला है,
आज हृदय में और सिंधु में
साथ उठा है ज्वार।
तूफानों की ओर घुमा दो,
नाविक, निज-पतवार ।
सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी।
बूढे भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी।
(2) धर्मवीर का उदाहरण –
जनि डरपहुँ सुर-सिद्ध सुरेसा।
तुमहिं लागि धरिहौं नरवेसा ।
अंशन सहित मनुज अवतारा।
लैहौं दिनकर-वंश उजारा।
हरिहौं सकल भूमि गरुआई।
निर्भय होहु देव-समुदाई।
इसमें विपक्षी को नीचा दिखाने के लिए और धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेने और कठिन कार्य करने में निहित उत्साह स्थायीभाव है। आलम्बन आश्रय – हरि। विषय – सुर-सिद्ध सुरेसा और देव-समुदाई। उद्दीपन विभाव -` भूमि गरुआई (तात्पर्य है – अत्याचारी व्यक्तियों के अत्याचार), देवताओं – का डरना। अनुभाव – जनि डरपहुँ, निर्भय होहु, हरिहौं, अवतार लेना। संचारी भाव – कार्य करने की दृढ़ता।
(3) दयावीर का उदाहरण –
देखि सुदामा की दीन दशा,
करुणा करि कै करुणानिधि रोये।
पानी परात को हाथ छुयो नहिं,
नैनन के जल से पग धोये।
यहाँ स्थायी भाव – उत्साह। आलम्बन विभाव – आश्रय – कृष्ण, विषय – सुदामा । उद्दीपन विभाव = सुदामा की दीन दशा। अनुभाव – नयनों के जल से पैर धोना। संचारी भाव = करुणा ।
(4) दयावीर का उदाहरण –
भामिनी देहुँ द्विजहिं सब लोक,
तजौ हठ मोरे यहै मन भाई ।
कृष्ण सुदामा को तीनों लोक देने के इच्छा रुक्मणी से बताते हैं। यहाँ स्थायी भाव = उत्साह। आलम्बन विभाव = आश्रय – कृष्ण, विषय – सुदामा। उद्दीपन विभाव = सुदामा की दरिद्रता। अनुभाव = दान देने की उत्सुकता। संचारी भाव = हर्ष ।