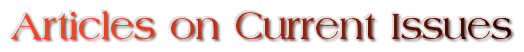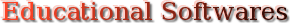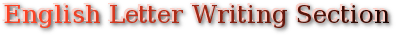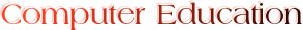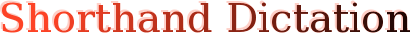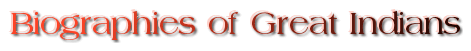Bharatiya Banking ki Sambhavnaye “भारतीय बैंकिंग की सम्भावनाएं” Hindi Essay 1000 Words for Class 10, 12 and Higher Classes Students.
भारतीय बैंकिंग की सम्भावनाएं
Bharatiya Banking ki Sambhavnaye
किसी भी समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास का आकलन उसकी बैंकिंग तथा भुगतान निपटान व्यवस्था के विकास से किया जा सकता है। बैंकिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले लगभग दो दशकों में हमारे आसपास बहुत कुछ बदला है, लेकिन जिस गति से बैंकिंग परिदृश्य बदला, वह अभूतपूर्व है। “बैंकिंग परिदृश्य में ग्राहक सेवा निरन्तर बदलते हुए अंततः किस स्वरूप को प्राप्त करेगी, इस बात का अनुमान लगाना किसी विचारशील बैंकर की कप्लपनाशीलता का अंत नहीं कहा जा सकता है। साथ ही यह एक चुनौती से भी कम नहीं है।”
भारतीय बैंकिंग का इतिहास
आजादी से लेकर आज तक के बैंकिंग के इतिहास को 4 विभिन्न चरणों में बाँटा जा सकता है। सन् 1947 से सन् 1969 तक की बैंकिंग का दौर उच्चवर्गीय बैंकिंग कहा जाता है इस दौर की बैंकिंग आम जनता की सुविधा एवं समृद्धि की प्रवर्तक होने के बजाय कुछ चुने हुए उच्चवर्गीय संस्थानों एवं नागरिकों के लाभार्थ होने के दायरे में सीमित थी।
सन् 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ भारत में संगठित बैंकिंग का प्रादुर्भाव हुआ जिसके तहत् राष्ट्रीयकृत बैंकों को वृहद स्तर पर भारत में गरीबी एवं विपन्नता के निराकरण हेतु अपनाए गए उपायों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम बनाया गया। भारतीय बैंकिंग व्यवसाय ने देश के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में अपने योगदान का जो उदाहरण पेश किया। उसकी मिसाल विश्व के किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है। इस दौर में बैंकिंग का आधिकाधिक झुकाव लाभप्रदता के बजाय सामाजिक सेवा के उद्देश्यों की ओर रहा। 15 अप्रैल, 1980 को 6 अन्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त देश के 20 राष्ट्रीयकृत बैंकिंग संस्थान अभूतपूर्व शाखा विस्तार के माध्यम से रोजगारजनक एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को देश के सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुँचाने के प्रयास में लग गए। एक सकारात्मक भूमिका निभाने के बावजूद इस दौर की बैंकिंग में जहाँ प्रतियोगिता का पूर्ण अभाव था, वहीं तकनीकी विकास की गति भी अति क्षीण थी। सरकारी क्षेत्र के बैंक ही बैंकिग परिदृश्य पर छाए थे और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं में कोई अंतर नहीं था। परिचालन की दृष्टि से बैंकों की लगभग समस्त गतिविधियाँ रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित थी। जिसके कारण बैंकों में प्रतियोगिता न के बराबर थीं एवं किसी भी अन्वेषण या नवोन्मेष की अभिप्रेरण का पूर्ण अभाव था।
1990 के दशक में बैंकिंग के एक नए स्वरूप का जन्म हुआ जिसे प्रूडेन्शियल या विवेकपूर्ण बैंकिग का नाम दिया गया 1990 का दशक आर्थिक एवं वित्तीय सुधारों की आँधी लेकर आया जिसने परम्परागत सामाजिक बैंकिंग को जड़ों से हिला कर रख दिया। आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण के नए नियमों ने न केवल बैंकों को पारदर्शी होने पर मजबूर किया, बल्कि कार्यक्षमता, गति एवं लाभप्रदता में सुधार को उनके अस्तित्व की एक अनिवार्य शर्त बना दिया, नई पीढ़ी के निजी बैंकों एवं विदशी बैंकों ने जोकि मूलतः लाभप्रदता के सिद्धान्त पर आधारित थे, बैंकिंग सेवाओं एवं उनको प्रदान करने के तरीकों में एक क्रान्ति ला दी। निजी एवं विदेशी बैंकों के भारतीय अर्थव्यवस्था में पदार्पण ने तकनीक एवं वैयक्तिक ग्राहक सेवा की नींव डालते हुए न सिर्फ ग्राहक वर्ग की अपेक्षाओं को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया, वरन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अपने स्तर से ऊपर उठ कर इन मापदण्डों पर अपने समकक्ष आने की चुनौती भी पेश की।
सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तकनीक, ग्राहक सेवा एंव लाभप्रदता जैस मुद्दों पर अपने से छोटे आकार के किन्तु सशक्त प्रतिस्पर्धी, निजी एवं विदेशी बैंकों से अपनी बराबरी का ऐलान किया। विवकपूर्ण बैंकिंग का यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण किन्तु सुखद आश्चर्य से भरा दौर था जिसमें जिनी एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने साथ-साथ लगभग एक रफ्तार से अनुत्पादक आस्तियाँ घटाने, तकनीक के माध्यम से अपनी पहुँच बढ़ाने, परिचालन लागत कम करने तथा नवोन्मेषी उत्पादों के जरिए अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए, भारतीय बैंकिंग इकाइयाँ विश्व की सबसे सशक्त बैंकिंग के दौर की अवस्थता से उठकर 1990 के दशक में बैंकों की प्राथमिकता स्वयं को सशक्त बनाने की थी। खुदरा बैंकिंग के माध्यम से बेहतर लाभप्रदता एंव सशक्तीकरण हासिल करने की दौड़ में इस बार मुख्यतः शहरी व मेट्रो केन्द्रों के ग्राहक बैंकों के व्यवसाय का केन्द्र रहे। जिसके परिमाणस्वरूप भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग बैंकिंग सुविधओं से वंचित रहा।
भविष्य की सम्भावनाएं
आधुनिक परिवेश में भारतीय बैंकिंग के इतिहास का एक नया अध्याय आरम्भ हुआ जिसे तकनीकयुक्त, नवोन्मेषी एवं सन्तुलित बैंकिंग का नाम दिया जा सकता है। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के कारण उसके स्वयं के नागरिकों की उत्पादों एंव सेवाओं की वृहद, विस्तृत एंव सशक्त माँग देश में उत्पादन का उच्च स्तर एवं विकास दर बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। भारत की निरंतर बढ़ती मध्यम वर्गीय जनसंख्या भारत की उच्च विकास दर की गारण्टी भी है और चुनौती भी। इस गारण्टी को और मजबूत बनाने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि भावी आर्थिक विपदाओं से भी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो, यह आवश्यक समझा जा रहा है कि भारत में वित्तीय वंचन से वित्तीय समावेशन की निर्विघ्न यात्रा आरम्भ हो। भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार की पहल से यह यात्रा आरम्भ हो चुकी है जिसका केन्द्रबिन्दु ग्राहक है। ग्राहक संतुष्टि एवं उत्तम ग्राहक सेवा आज की पहली जरूरत बन गई है जिस पर सामूहिक प्रयास आरम्भ हो चुके हैं।
एशिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्था में भारत ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था का इन्जन’ कहा जाता है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मॉडल ज्यादा सशक्त एवं टिकाऊ साबित होने वाला है, क्योंकि भारत की विकास दर का मुख्य आधार निरंतर बढ़ता घरेलू उपभोक्ता बाजार है जिसके केन्द्र में बढ़ते स्थायी ग्राहक हैं, इसलिए भी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा महत्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त आगमी वर्षों में भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग अपेक्षाकृत कम एवं क्रियाशील उम्र का होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस सशक्त पक्ष को ‘जनांकिकीय लाभांश’ (डेमोग्राफिक डिविडेंड) का नाम दिया जाता है।