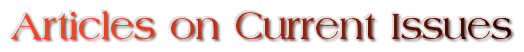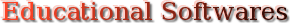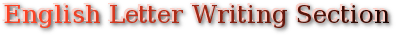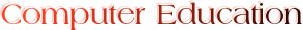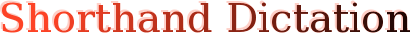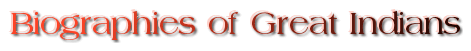Suchna ka Adhikar “सूचना का अधिकार” Hindi Essay, Paragraph in 800 Words for Class 10, 12 and competitive Examination.
सूचना का अधिकार
Suchna ka Adhikar
लोकतांत्रिक देशों में स्वीडन पहला देश था जिसने अपने देश के लोगों को 1766 ई. में ही सांवैधानिक रूप से सूचना का अधिकार प्राप्त कराया। आज नीदरलैण्ड, आस्ट्रिया और अमेरिका आदि देशों के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है।
भारत में सूचना के अधिकार की विकास यात्रा 1952 ई. से शुरू होती है जब भारत में पहला प्रेस आयोग बना। सरकार ने आयोग व प्रेस की स्वतंत्रता सम्बन्धी जरूरी प्रावधानों पर सुझाव माँगा। उसके बाद सन् 1967 में सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन के प्रस्ताव आए, लेकिन उन प्रस्तावों को खारिज कर इस कानून को और सख्त बना दिया गया। 1977 में जनता पार्टी में अपने चुनाव घोषणा-पत्र में सूचना का अधिकार देने का वादा किया। 1978 में प्रेस आयोग बना। इस प्रेस आयोग ने और 1968 में बनी प्रेस परिषद् ने कुछ सिफारिशें की लेकिन नतीजा नहीं निकला। लोगों तक सूचना पहुँचाने की दिशा में सार्थक प्रयास 1989 में बनी वी. पी. सिंह सरकार ने किया। 1996 के लोकसभा चुनाव में लगभग सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने घोषणा-पत्र में सूचना के अधिकार से सम्बन्धित कानून बनाने की बात की। सिलसिला आगे बढ़ा और 1997 में इस सम्बन्ध में दो विधेयक लाए गए। एक विधेयक पत्रकार अरुण शौरी के पिता एच. डी. गौरी ने बनाया था। और दूसरा प्रेस परिषद् के अध्यक्ष जस्टिस सावंत के नेतृत्व में गठित कार्यदल ने बनाया था। लेकिन ये दोनों विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले सके। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की देवगौड़ा और गुजराल की सरकार तो आईं और गईं। इस पर पुनः कुछ न हो सका। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में कानून पास किया लेकिन इसमें इतनी खामियां थीं कि यू. पी. ए. सरकार को दोबारा विधेयक तैयार करना पड़ा।
सूचना के अधिकार से सम्बन्धित जो प्रावधान है उसके अन्तर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय और अधिकारी से जवाब-तलब कर सकेगा। सरकारी फाइलों को देखने, उससे नोट्स लेने, उनकी फोटो कॉपी लेने का अधिकार होगा। अगर जानकारी कम्प्यूटर पर हो तो प्रिंट आऊट या फ्लापी मिल सकेगी। माँगी गई सूचना 30 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना कानूनन जरूरी होगा। किसी की जिन्दगी या आजादी से जुड़ी सूचना 24 घण्टे में देनी होगी। सभी मंत्रालय और विभाग इस काम के लिए खासतौर पर जन सूचना कोषांग नियुक्त करेंगे। हर राज्य में चुनाव आयोग की तरह मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय होगा। जरूरी सूचना न मिलने पर मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय में शिकायत की जा सकती है।
लेकिन सूचना के अधिकार से सम्बन्धित इस कानून में कुछ मर्यादाएँ भी निर्धारित की गई हैं। ‘रॉ’ और आई. बी. जैसी खुफिया एजेन्सियों को अपने राज बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताकर सूचनाएं छुपाई भी जा सकती हैं। राजस्व, गुप्तचर निदेशालय को भी इसी प्रकार की छूट दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि अर्द्धसैनिक बलों की गतिविधियाँ तथा ऐसी सूचनाएँ जिससे केन्द्र और राज्यों के रिश्ते प्रभावित हों, को भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों की ओर से फाइल पर लिखी गई नोटिंग देखना भी इस कानून के तहत संभव नहीं होगा। अपराध रोकने या कानून व्यवस्था लागू करने का मामला हो तो प्रावधान किया गया है कि वह जानकारी नहीं दी जाएगी जो किसी व्यक्ति की निजता भंग करती हो, इस कानून में यह प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को सूचना देने से मना करता है या देर से अथवा गलत सूचनाएँ देता है तो वह अधिकारी निजी तौर पर दण्ड का भागीदार होगा।
इस कानून का नाम ‘सूचना की स्वतंत्रता’ के बजाय ‘सूचना का अधिकार’ रखा गया है। अतः यह लोगों को केवल स्वतंत्रता ही नहीं देता बल्कि उन्हें अधिकार सम्पन्न भी बनाता है। लेकिन इस कानून में जिन क्षेत्रों की बात कही गई है वह कानून की मूल आत्मा को ही खंडित कर देता है। मौजूदा कानून में ऐसे कुल 50 क्षेत्रों का उल्लेख है जिनसे सम्बन्धित सूचनाएँ हमेशा गोपनीयता के दायरे में रखी जाएगी। इनमें ऐसी सूचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। जिसको देने से भारत की सम्प्रभुता, अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, राजनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों तथा विदेशों से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हों। सवाल यह उठता है। कि यह तय करने का अधिकार किसे होगा कि अमुक सूचना देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के लिए गुप्त रखी जाएगी। जाहिर है कि मौजूदा कानून इसका अधिकार सूचना आयुक्तों को ही देता है। इससे अफसरशाही के नए तंत्र के विकसित होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात यह कि सूचनाएं मिलने पर सूचना माँगने वाले व्यक्ति के पास एक ही रास्ता है-छोटे से शुरू होकर बड़े सूचना आयुक्त के कार्यालय में शिकायत करना और अंततः न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना। तीसरी बात यह भी है कि भूमण्डलीकरण और निजीकरण के इस दौर में भी सूचना का अधिकार देने वाला यह विधेयक निजी क्षेत्र को अपने दायरे में नहीं रखता है।