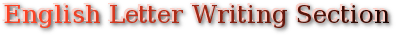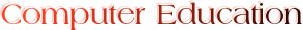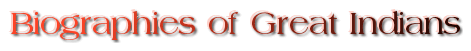Hindi Essay, Paragraph, Speech on “Pustak Pradarshani”, ”पुस्तक प्रदर्शनी ” Complete Hindi Anuched for Class 8, 9, 10, Class 12 and Graduation Classes
पुस्तक प्रदर्शनी
राजधानी दिल्ली का प्रगति मैदान एक ऐसा स्थान है, जहाँ अक्सर एक-न-एक प्रदर्शनी चलती ही रहती है। इस कारण वहाँ अक्सर भीड़-भाड का बने रहना भी ना स्वाभाविक है। प्रदर्शनी कोई हो या न हो; पर वहाँ अक्सर कई तरह के साँस्कृतिक कार्यक्रम नाटक, फिल्म शो, रंगारंग कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं। फिर साथ ही बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क अप्पू घर भी है। इसलिए मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ। लेकिन पिछले वर्ष जब मैंने सुना, समाचारपत्रों में पढ़ा भी कि इस बार वहाँ प्रगति मैदान में एक अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, तो पुस्तक-प्रेमी होने के कारण सिर्फ एक दिन नहीं, मैं लगातार तीन दिनों तक वहाँ जाता रहा। वास्तव में मेला और प्रदर्शन-स्थल इतना विस्तृत था, दूसरे इतने अधिक प्रकाशकों ने वहाँ पर अपने स्टॉल लगा रखे थे, कि सब को मात्र एक दिन में देख पाना संभव ही नहीं था। सोचा था कि एक दिन न सही, दो दिनों में पूरा देख लँगा; पर नहीं, मुझे वहाँ तीसरे दिन भी जाना पड़ा।
पहले दिन तो हम सभी सहपाठी अपने विद्यालय की ओर से एक अध्यापक महोदय के साथ गए। इस कारण टिकट आदि में रियायत मिल गई, पर कोशिश करने पर भी हम लोग पूरी प्रदर्शनी तो क्या मात्र हिन्दी-विभाग को भी पूरा नहीं देख पाए। कुछ सहपाठी तो अवश्य जल्दी मचाते रहे; पर प्रदर्शित की गई पुस्तकों के आकार-प्रकार, रूप-रंग और शीर्षक आदि इतने मोहक थे कि मेरे लिए एक-एक स्टॉल पर रखी प्रत्येक पुस्तक को देखना बहुत जरूरी हो गया था। सो अध्यापक महोदय और साथी कहीं आगे निकल गए, जबकि मैं पीछे पुस्तकें देखता हुआ अकेला ही रह गया। स्टॉल पर खड़े कर्मचारी से मैं पुस्तकों, उनके विषयों, छपाई आदि के बारे में कई तरह के प्रश्न भी पूछता रहा। वे लोग बड़े प्रेम से मुझे सब कुछ बताते रहे। मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी भी। मेरी उत्सुकता और प्रश्नों से कुछ तो इतने खुश हुए कि मुझे दस प्रतिशत के बदले बीस-पच्चीस प्रतिशत तक कमीशन दे दिया। कुछ ने तो आधी कीमत ही ली। कुछ ने छोटी-छोटी दो-तीन। पुस्तकें मुफ्त में ही दे दीं।
चाहता था कि अभी और देखता रहूँ, पर समय अधिक हो जाने के कारण घर वाले चिन्ता न करें, इस कारण मन ही मन कल फिर आने की बात सोच वहाँ से बाहर आया. बस पर बैठा और घर आ गया।
अगले दिन शनिवार था। स्कूल से छुट्टी जल्दी हो गई। हम तीन-चार साथियो ने घर वालों से आज्ञा ली और प्रदर्शनी-स्थल पर आ पहुँचे। पता नहीं क्यों, पुस्तक-प्रदर्शनी स्थल पर जाने से पहले हम लोग अपने किशोर-मन को अप्पू घर जाने से रोक नहीं पाए। जब वहाँ का मनोरंजन करते एक घण्टा हो गया, तो साथियों को लगातार घसीटता हुआ-सा प्रदर्शनी स्थल पर ले गया। अप्पू घर की तरफ से घुसने का दण्ड भी हमें भोगना पड़ा. वह यह कि प्रदर्शनी स्थल पर जाने के लिए एक तो टिकट नया खरीदना टसरे चलना भी काफी पड़ गया। खैर, पुस्तकों की दुनियाँ में पहुँच कर मुझे वह याद नहीं रहा और मैं फिर एक बार रंग-बिरंगी पुस्तकें देखने में खो गया।
कई जगह कुछ प्रकाशक अपने सूचीपत्र बाँट रहे थे और कुछ लोग अपनी विशेष स्तकों की इश्तिहारबाजी भी कर रहे थे। कुछ प्रकाशक छोटी-छोटी पत्र-पत्रिकाएँ भी लाँट रहे थे। कइयों ने अपने प्रकाशकों के नाम से प्लाटिक के थैले से बनवा रखे थे। सो वे अपनी प्रचार सामग्री उनमें भर कर बाँट रहे थे। एक-दो स्टालों पर विशेष रूप से चर्चित पुस्तकों के लेखक भी मौजूद थे, जो खरीददारों को अपनी पुस्तकों पर अपने हस्ताक्षर करके दे रहे थे। मैंने यह भी अनुभव किया कि आम तौर पर पुस्तकें उलट-पलट कर देखने वालों की संख्या अधिक थी, खरीदने वालों की कम। इस का कारण यह भी हो सकता है कि पुस्तकों पर लिखी कीमतें इतनी अधिक थीं कि पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग चाह कर भी उतनी कीमत पर पुस्तकें खरीद पाने में अपने को समर्थ नहीं पा रहे थे। जो हो. आज हम प्रदर्शनी का हिन्दी-विभाग पूरा देखकर ही बाहर आए।
तब तक शाम हो चुकी थी। सर्दी कुछ बढ़ गई थी। हम लोग थक भी गए थे। सो पहले हमनें एक चाय के स्टॉल पर पहुँच कर चाय पी, समोसे भी खाए उनकी कीमत तो पुस्तकों से भी बढ़ कर महँगी थी; पर आदमी भूखा तो रह नहीं सकता। सो कड़वा धूट भरना ही पडा। बाहर आकर बस की और घर आ गए।
अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। सो हम लोग सुबह दस बजे ही प्रदर्शनी स्थल पर आ पहँचे। आज हमने अप्पू घर वाले गेट से भीतर आने की गलती नहीं दोहराई। जिस भाषा को हम अच्छी तरह बोल, समझ और पढ़-लिख सकते थे, उस हिन्दी-विभाग का प्रदर्शनी तो देख ही चुके थे। सो आज अन्य भाषाओं, अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं का पुस्तकों की प्रदर्शनी देखने में अधिक देर नहीं लगी। यहाँ भी यदि भीड थी, तो अंग्रेजी पुस्तकों के स्टॉल पर ही थी, बाकी सभी के कर्मचारी तो प्रायः ऊँघ रहे थे। हाँ, व्यवहार उन्हीं का सब से मधुर और सभ्य और शिष्ट था, जबकि अंग्रेजी वालों की गर्दनें ऐंठी हुई लग रही थीं। जहाँ तक पुस्तकों की कीमतों का प्रश्न है, हिन्दी की तुलना में अग्रेजी-पुस्तकों की कीमतें काफी सन्तुलित, बल्कि कम थीं।
जल्दी फुर्सत पा जाने के कारण हमने ‘शाकुन्तलम’ में चल रहा एक नाटक भी देखा और वापिस आ गए। पुस्तकों का वह विशाल संसार आज भी मेरे मन-मस्तिष्क में प्रदर्शित होता रहता है।